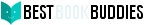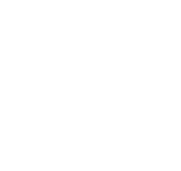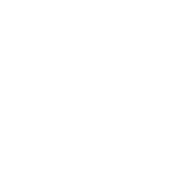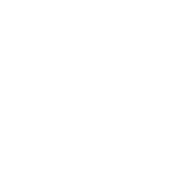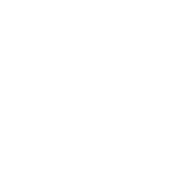साहित्य- समय बनाम लेखकीय दायित्व - पंकज पराशर
लोगों को केन सारो वीवा की तरह फांसी पर लटका दिया गया, सुकरात की तरह जहर का प्याला दिया गया और अनेक देशों में अनेक क्रांतिकारी लेखकों को जेल में डाल कर अमानवीय यातनाएं दी गई। उनकी किताबों को प्रतिबंधित कर दिया गया।
इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्ता जब सिर्फ ताकत और दमन के दम पर राज करती है, तो अधिकतर लेखक-कलाकार या तो मौन होने लगते हैं या शाश्वत किस्म के विषय जैसे- मृत्यु, संसार, ईश्वर, दर्शन, चिड़िया, फूल, प्रकृति और नारी-देह के नख-शिख वर्णन के राजमार्ग पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गिने-चुने ही सही, कुछ जिद्दी और जुनूनी किस्म के घरफंूककवि-कलाकार भी हर काल में होते रहे हैं, जो सच को सच कहने से बाज नहीं आते, यथासंभव सच के हत्यारों की शिनाख्त करते हैं, अपनी कला और रचना द्वारा प्रतिरोध करते हैं। मगर यह सवाल बार-बार उभरता है कि जिस हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरे गाजे-बाजे के साथ ‘हिंदी नवजागरण’ चलता रहता है, उस समाज के तत्कालीन निवासी ‘हिंदी जाति’ के लेखकों ने 1857 के विद्रोह की भयावहता और अमानवीयता को डायरी, आंखों देखा हाल या विश्लेषण के रूप में कहीं दर्ज क्यों नहीं किया है? माना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तब महज सात साल के बालक थे, लेकिन राजा शिवप्रसाद ‘सितारे-हिंद’ भी तो तमाम मुद्दों के प्रति एकदम खामोश और निरपेक्ष नजर आते हैं! सदासुखलाल, पंडित युगलकिशोर, लल्लूलाल, सदल मिश्र सरीखे हिंदी के पुरोधा तब जीवित और होशमंद थे, जब गदर के विद्रोह ने हिंदी जाति को तबाहो-बर्बाद किया था।
अंग्रेजी राज में नई राजस्व प्रणाली के तहत परंपरागत भूस्वामी वर्ग के तहस-नहस हो जाने, नए ताल्लुकेदारों के अधिकारों को खत्म करने, अंग्रेजों द्वारा रियासतों को हड़पने, लखनऊ में सरकारी फौजों की लूटमार, 1857 तक अंग्रेजों के सौ बरस के शासन में भारत में परंपरागत वर्गों की तबाही आदि को लेकर उनके यहां सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं मिलता। यही नहीं, सवाल यह है कि हिंदी साहित्य में 1857 के विद्रोह के दौरान और उसके कुछ सालों के बाद भी कोई स्तरीय या स्तरहीन रचना थोड़ी संख्या में भी क्यों नहीं मिलती? माना कि उस वक्त हिंदी में कम लेखक थे और जो थे, उनके भीतर वैसी राजनीतिक सजगता और चेतना नहीं थी। लेकिन 1947 के भारत विभाजन के दौरान जिस तरह के भयानक दंगे, आगजनी, विस्थापन और बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ, क्या उस पर हमारे हिंदी साहित्य के राजनीतिक रूप से सजग और संवेदनासंपन्न लेखकों ने कुछ लिखा है? प्रगतिवाद के क्रांतिकारी तमाम सूरमा कवि जीवित थे, छायावाद के तीन पुरोधा भी तब हयात ही थे, प्रयोगवादियों की कलम भी तब यकीनन बंद नहीं थी। जब हिंदुस्तान में लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, लाखों इधर से उधर हुए, उस देश के हिंदी साहित्य में सिवाय मौन और सन्नाटे के इस विषय पर और क्या चीजें हमें मिलती हैं? गिनाने को अज्ञेय की कुछ कहानियां गिना देंगे! और किन-किन लेखकों का क्या इन दो बड़ी घटनाओं पर मिलता है?
विडंबना देखिए कि हिंदी भाषा के सवाल पर बहस करते हुए जिस उर्दू को लेकर आधुनिक हिंदी साहित्य में जमाने भर की बातें मिलती हैं, उस उर्दू में 1857 के विद्रोह के समय की सत्ता की क्रूरता और अमानवीयता का न केवल चश्मदीद बयान/ दस्तावेज मिलता है, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बिना डरे, बिना खौफ खाए उन्हें उनकी गलतियां बताने का दुस्साहस भी दिखाई देता है। मसलन मिर्जा गालिब की फारसी में लिखी डायरी ‘दस्तंबू’, जहीर देहलवी की ‘दास्तान-ए-गदर’, जकाउल्ला खां की ‘तारीख-ए-हिंद’, ‘रोजनामचा-ए-गदर’ और सर सैयद अहमद खां की किताब ‘असबाबे-बगावते-हिंद’ में सैयद ने विद्रोह के ठोस कारणों को तर्कसंगत ढंग से गिनाया था। यहां इस सवाल पर जरा संजीदगी से गौर कीजिए कि सन 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने जैसी कू्ररता और भयानक अमानवीयता दिखाई थी, क्या उस भय का इतना व्यापक असर रहा कि हिंदी साहित्य के लेखक आगे भी कभी मुंह खोलने की जुर्रत नहीं कर पाए? या मुसलमानों की तरह हिंदू 1857 के विद्रोह में व्यापक धन-जन हानि के शिकार नहीं हुए थे? तथ्य यह है कि बदले की भावना से भरे हुए अंग्रेजों ने अपनी राह में आने वाले किसी को नहीं बख्शा था। वे चाहे हिंदू रहे हों, या मुसलमान, चाहे अंग्रेजों के समर्थक रहे हों या विरोधी। दूसरी बात, 1947 के लोकतांत्रिक भारत में देश-विभाजन की पीड़ा को व्यक्त करने में किस सत्ता से दमन और प्रताड़ना की आशंका ने हिंदी लेखकों को कलम उठाने से रोक रखा था? जबकि अब्दुल्ला हुसैन ने ‘उदास नस्लें’ लिखीं, इंतिजार हुसैन ने ‘बस्ती’, बप्सी सिधवा ने ‘द आइस कैंडी मैन’, सआदत हसन मंटो ने मुसलसल लिखना जारी रखा। अगर एक ही भाषा (वन लैंग्वेज ऐंड टू स्क्रिप्ट- क्रिस्टोफर किंग) थी, तो लिपि बदलते ही लेखकों के विचार, संवेदना और साहस सब कुछ इतना अलग कैसे हो गया? जो बातें फारसी लिपि में कही जा सकती थीं, वे देवनागरी में क्यों नहीं अभिव्यक्त हो सकीं?
आज जब मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया में भी अपने को व्यक्त करने के मौके हैं, अधिकतर व्यावहारिक और चतुर-सुजान लेखकों-कलाकारों को क्यों सांप सूंघ गया है कि वे या तो चुप्पी को बेहतर समझते हैं या ‘संधा-भाषा’ में गोया यूं बोलते हैं, ‘बक रहा हूं जुनूं में क्या क्या कुछ/ कुछ न समझे खुदा करे कोई’? 1943 के बंगाल के अकाल के प्रमुख चित्रकारों के रूप में हम जैनुल आबेदिन, चित्तप्रसाद, रामकिंकर बैज, सोमनाथ होड़, गोबर्धन आश, देबब्रत मुखोपाध्याय आदि को पाते हैं। पर यह सच है कि इनके अलावा तमाम और चित्रकार भी थे, जिन्होंने अकाल पर चित्र बनाए थे। लेखकों की एक बड़ी बिरादरी हिंदी क्षेत्र में है। पुरस्कारों और सम्मानों और तालियों की गूंज से आगे का वक्त आ चुका है। याद रहे कि जब आपका सम्मान, आपकी कविता, कहानी और लेख को याद किया जाएगा, उसी समय आपके समय के उजालों की हत्या का भी जिक्र किया जाएगा और इस हत्यारे पल के खिलाफ आपकी भूमिकाएं भी पूछी जाएंगी। अपने समय के सवालों से घबरा कर मौन को चुन लेने वाले जब मर कर भी अपने समय के सवालों से इतिहास में घिर जाएंगे, तब कहां जाकर चैने पाएंगे?